विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न हदों तक कृषि ऋणों की माफी के आशय की घोषणाओं की मीडिया और अन्य टिप्पणीकारों द्वारा सख्त आलोचना की गई है। इस आलेख में डॉ. प्रनब सेन ने उन दावों की वैधता की जांच की है जिन पर यह विरोध आधारित है।
पिछले दो महीनों में भारत में पिंक प्रेस विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई कम या अधिक हद तक कृषि ऋणों की माफी के इरादों की अनेक घोषणाओं के खिलाफ बरस पड़े हैं। यह सब उत्तर प्रदेश में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री द्वारा अपने दल के घोषणापत्र के अनुरूप अपनी पहली वास्तविक आर्थिक घोषणा करने से शुरू हुआ, हालांकि उस समय तक उत्तर प्रदेश के किसानों ने ऐसी कोई पुरजोर स्पष्ट मांग नहीं की थी। उसके बाद से पूरे देश में किसानों के आंदोलन और उनकी आत्महत्याओं में हुई वृद्धि से एक के बाद एक राज्य सरकारें किसानों के संकट में कमी लाने के गंभीर विकल्प के रूप में इस पर विचार करने के लिए बाध्य हुई हैं।
काफी आश्चर्य की बात है कि मीडिया और अन्य टिप्पणीकार किसानों के संकट की वास्तविकता को तो कबूल करते हैं लेकिन समस्या समाधान के उपाय के रूप में कृषि ऋण की माफी पर गंभीर आपत्तियां खड़ी करने लगते हैं। भारत के कुलीनों द्वारा इस संबंध में अपनाई गई स्थिति का सारांश भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के शब्दों में सबसे बेहतर ढंग से व्यक्त हुआ है : ‘‘मैं सोचता हूं कि यह (कृषि ऋण माफी) ईमानदार ऋण की संस्कृति को कमजोर करती है, ऋण अनुशासन को प्रभावित करती है, भविष्य में ऋण लेने वालों द्वारा ऋण चुकाने की पहलकदमियों को कुंद करती है। दूसरे शब्दों में, ऋण माफियों से नैतिक जोखिम पैदा होता है। अंत में इसका परिणाम करदाताओं से ऋणी लोगों को अंतरण के रूप में होता है। अगर इसके कारण सरकार द्वारा समग्रतः लिया जाने वाला उधार बढ़ जाता है, तो सरकारी बांड पर प्रतिफल भी प्रभावित होते हैं। उसके बाद, इसके कारण निजी ऋण लेने वाले बाहर कर दिए जाते हैं क्योंकि सरकार द्वारा अधिक उधार लेने के कारण दूसरों के लिए उधार लेने का खर्च बढ़ जाता है। मेरा सोचना है कि हमें इस तरह का मतैक्य स्थापित करना चाहिए जिसमें ऋण माफी के वादों से बचा जाय, अन्यथा इस संबंध में निम्न स्वायत्तता वाली (सब-सॉवरेन) राजकोषीय चुनौतियां राष्ट्रीय बैलेंस शीट को प्रभावित कर सकती हैं।’’ (संवाददाता सम्मेलन, 6 अप्रैल, 2017)।
ये अनिष्टसूचक शब्द हैं। नई और डरावनी शहरी दंतकथा रचने के लिए विभिन्न वक्ताओं द्वारा इस विचार के अलग-अलग पहलुओं को चुना गया है। चिंता की बात यह है कि जिस खास संदर्भ में इन ऋण माफियों पर विचार किया जा रहा है, उस संदर्भ में इन दावों की वैधता की गंभीर जांच करने की जहमत उठाते हुए कोई भी नहीं दिखता है। संभवतः इसीलिए यह ऐसा करने का समय है।
जिस पहले बिंदु को उठाने, और जोरदार ढंग से उठाने की जरूरत है, वह यह है कि कृषि ऋण माफी देने का यह कोई पहला मौका नहीं है। अतः इसके प्रभावों का अनुभव आधारित सत्यापन करना संभव है। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसे प्रभाव सही भी हों, तो उनका मूल्यांकन इस प्रतितथ्य को सामने रखकर करने की जरूरत है कि - अगर ये ऋण माफियां नहीं दी जाती हैं, तो उनके संभावित परिणाम क्या होंगे? तीसरी, यह बात निश्चित तौर पर पूछी जानी चाहिए कि क्या बार-बार दी जाने वाली ये ऋण माफियां अविचारित राजनीतिक लोकप्रियतावाद के लक्षण हैं या ये भारत में कृषि ऋण की संरचना में मौजूद कहीं अधिक बुनियादी समस्या का संकेत देते हैं?
ऋण की संस्कृति और नैतिक जोखिम
किसानों द्वारा कर्ज चुकाने की इच्छा पर माफियों के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए हमें बहुत पीछे की बातों पर सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा अंतिम मामला 2009-10 का है जब देश पिछले 35 वर्षों में पड़े सबसे भयंकर सूखे से पीडि़त था। उसके बाद से आठ वर्ष बीत गए लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि कृषि ऋण अदायगी में किसी तरह की सुस्ती आई है या ऋण माफियों की बार-बार मांग की जा रही है - यहां तक कि 2014-2016 की अवधि में लगातार दो वर्षों तक पड़े सूखे के दौरान भी नहीं। यह तथ्य वास्तव में अतीत में प्रत्येक कृषि ऋण माफी के बाद सही साबित हुआ है। दूसरे शब्दों में, इस प्रस्थापना को कोई अनुभवसिद्ध समर्थन प्राप्त नहीं है कि ऐसी ऋण माफियों से ‘‘ऋण संस्कृति’’ को गंभीर नुकसान होता है। बिना किसी अनुभवसिद्ध साक्ष्य के इस तर्क को सैद्धांतिक प्रस्थापना के रूप में उछालना शुद्ध रूप से वक्ताओं के रूझान के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है।
तो क्या इसका अर्थ यह है कि भारतीय किसान नैतिक रूप से उन आर्थिक मानवों से बेहतर हैं जिनके व्यवहार को आधार बनाकर ‘नैतिक जोखिम’ की अवधारणा प्रतिपादित की गई है; या यह बात है कि इस सिद्धांत का उपयोग ही गलत ढंग से किया जा रहा है? नैतिक मानकों पर विचार किए बिना भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस सिद्धांत का गलत उपयोग किया गया है। ऋण संस्कृति और नैतिक जोखिम मानव व्यवहार के अंग हैं जो ‘नियामकीय सहनशीलता’ के लिए अधिक प्रासंगिक है जिसका विस्तार भारतीय रिजर्व बैंक कृषि ऋण माफी के इस स्वरूप के बजाय कॉर्पोरेट ऋणों के मामले में सामान्यतया करता रहा है। ऐसी ऋण माफियां व्यक्तिगत रूप से किसानों को नहीं दी जाकर तृतीय पक्ष अर्थात सरकार द्वारा एक वर्ग के रूप में किसानों को दी जाती हैं। इसलिए अगर कोई किसान इस आशा में अपना कर्ज अदा नहीं करता है कि कर्ज माफ कर दिया जाएगा, तो सरकार द्वारा उपकृत नहीं करने पर वह खुद को ऋण संबंधी चूक के सामान्य परिणामों का भागी बना दे रहा है।
इतिहास को देखते हुए इस बात को पूछना प्रासंगिक है कि यह मांग अभी ही क्यों की जा रही है। क्या यह विकृत हो रही ऋण संस्कृति का सूचक है? इसका उत्तर है - नहीं। कृषि ऋण हेतु नीतिगत रूपरेखा में प्रावधान किया गया है कि जिन स्थितियों में केंद्र सरकार सूखे की घोषणा करती है, उनमें कृषि ऋणों को आरंभ में एक वर्ष के लिए और बाद में अधिकतम तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। यह कोई व्यापक प्रावधान नहीं है। यह आधिकारिक रूप से घोषित ‘प्रभावित जिलों’ में ही किसानों पर लागू होता है। सूखा वाले जिलों में पिछले कुछ वर्षों में इसी प्रावधान का उपयोग किया गया है, और उसके आधार पर किसानों के संकट को कुछ हद तक दूर किया गया है। लेकिन वर्ष 2016-17 की स्थिति भिन्न थी। उसमें कोई सूखा या प्राकृतिक आपदा की स्थिति नहीं थी। किसानों की समस्या लगभग पूरी तरह से विमुद्रीकरण (नोटबंदी) के कारण थी। इसका अर्थ हुआ कि उसकी कोई स्पष्ट भौगोलिक सीमा नहीं थी अर्थात व्यवहारतः सभी किसान उससे पीडि़त हुए हैं और उनके ऋणों को आगे नहीं बढ़ाया गया है। फलतः पूरे देश के किसान या तो आंदोलित हैं या चूक की आशंका झेल रहे हैं।
यह ऋण संस्कृति के कमजोर होने या नैतिक जोखिम का मामला नहीं है। यह महज इस तथ्य का परिणाम है कि: जहां सरकार ‘ईश्वरीय कृत्यों’ के लिए प्रावधान करना चाह रही है, वहीं ‘राजकीय कृत्य’ या ‘फोर्स मेजियर’ (अप्रत्याशित स्थिति) के लिए प्रावधान नहीं करना चाह रही है। अगर यह कुछ है तो राजसत्ता का अस्वीकार है।
अगर ऋण माफी नहीं हो, तो ...
उसके क्या आर्थिक परिणाम होंगे? भारत में बैंकों के कृषि ऋण अनिवार्यतः भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा बीमित होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि ऋण माफी नहीं होने पर बैंकों को कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि जो स्थिति बनती है, उसके अनुसार बैंकों के लिए कृषि बीमा कंपनी का बीमा किसी भी तरह से इस अर्थ में बीमांकिक (ऍक्चुअरियल) उत्पाद नहीं है कि अनुमानित नुकसान और लाभ समय के साथ ग्राहकों द्वारा समंजित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा, बीमा कंपनी के पास पूंजी की गंभीर कमी है और उसके पास बड़े पैमाने की चूकों को कवर करने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं हैं। उसकी देनदारियों को बजटीय सहायता के जरिए केंद्र सरकार द्वारा पूरा किया जाता है।
अतः जिन परिस्थितियों में किसानों का संकट व्यापक है और उसके कारण ऋण चुकाने में बड़े पैमाने पर चूक की आशंका है, उनमें केंद्र को कदम उठाना होगा और आवश्यक धनराशि उपलब्ध करानी होगी। इसमें भी ‘‘करदाताओं से ऋणी लोगों तक अंतरण’’ होगा और ‘‘समग्र सरकारी उधार’’ बढ़ेगा। अंतर यह है कि जहां ऋण माफियों का भार राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा, वहीं चूकों का भार केंद्र पर पड़ेगा। दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां माफियों से किसान की सारी देनदारी खत्म हो जाती है, वहीं चूकों के गंभीर परिणाम होंगे, जैसे कि कॉलेटरल दिया गया हो, तो उसका नुकसान, और भविष्य में बैंक से ऋण पाने की संभावना समाप्त होना।
इन विकल्पों की उपादेयता का मूल्यांकन करने पर दो बातें प्रासंगिक हो जाती हैं : पहला, सरकार द्वारा किए जाने वाले भुगतानों की मात्रा, और दूसरा, किसानों पर उसके परिणाम। ऋण माफी के विकल्प के साथ लगभग हमेशा ही ‘समावेश की त्रुटियां’ संलग्न होती हैं। इसके दायरे में वे किसान भी आ जाते हैं जिनके ऋण माफ करने की जरूरत नहीं होती। फलतः, चूक की स्थिति में सरकार द्वारा चुकाई जाने वाली रकम सामान्य विकल्प की अपेक्षा काफी बढ़ जाने की आशंका रहती है। अंततः, देखा जाए तो, सर्वाधिक संकटग्रस्त और सर्वाधिक असुरक्षित लोगों पर ही सर्वाधिक भार पड़ता है और उन्हें औपचारिक ऋण प्राप्ति की व्यवस्था से और संभवतः खेती से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है।
यह नैतिक मुद्दा भर नहीं है - इसके आर्थिक परिणाम भी होते हैं जिसके मामले में नीति निर्माताओं और टिप्पणीकारों ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। हमारी अधिकांश कृषि रणनीति भारतीय किसानों को पारंपरिक जीवन-निर्वाह कृषि से अधिक व्यावसायिक कृषि-कार्यों की ओर बढ़ने के लिए समझाने-मनाने पर आधारित है। पिछले लगभग दो दशकों से भी अधिक समय से ‘विविधीकरण’ सरकारी कृषि नीति का मूलमंत्र रहा है। यह किसानों की आजीविका में सुधार लाने की रणनीति भर नहीं है। यह ऐसे उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए भी अनिवार्य है जिनकी मांग आमदनी बढ़ने के साथ, खास कर शहरी क्षेत्रों में, बढ़ती जाती है। भारत में 2000 के दशक के मध्य से एक दशक तक खाद्य पदार्थों की महंगाई देखी गई है जो इस बात की पूर्वसूचना है कि कृषि विविधीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ने की स्थिति में क्या होगा।
जीवन-निर्वाह कृषि को छोड़ने पर किसानों को निश्चित तौर पर पहले से काफी अधिक निवेश करना और जोखिम लेना पड़ता है। कृषि वित्तव्यवस्था के साहूकार जैसे पारंपरिक स्रोत न तो उतनी रकम दे सकते हैं और न ही उतने मुनाफे की गुंजाइश दे सकते हैं कि जोखिम लेना उपयोगी हो सके। इसलिए बड़ी संख्या में किसानों को औपचारिक ऋण लेने से वंचित कर देने और उन्हें वापस साहूकारों के हवाले कर देने से कृषि के व्यवसायीकरण और विविधीकरण की प्रक्रिया को धक्का लगेगा जिसके खाद्य पदार्थों की महंगाई के मामले में स्पष्ट निहितार्थ होंगे।
पसंद स्पष्ट है : एक ओर तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा वर्णित कयामत का परिदृश्य है और दूसरी ओर, खाद्य पदार्थों की रुकी हुई महंगाई और उसके कारण चलने वाली सख्त मौद्रिक नीति है। इसलिए आर्थिक मोर्चे पर तो यह सर्वोत्तम पसंद लगती है लेकिन नैतिक मोर्चे पर यह बेवकूफी लगती है।
‘उप-स्वायत्त’ की दुविधा
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के शब्दों में निश्चित तौर पर एक ‘आपसे अधिक पवित्र’ वाली गंध आ रही है जिसकी प्रतिध्वनि वित्त मंत्री द्वारा ऋण माफी के मामले में राज्यों को सहायता देने से स्पष्ट इनकार करने में भी प्रतिध्वनित होती है। यह सनक से अधिक कुछ नहीं है। इसलिए कि इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान संकट मुख्यतः विमुद्रीकरण का परिणाम है, जिसमें वित्त मंत्री और गवर्नर, दोनो ही भागीदार थे। इस बात में प्रसिद्ध अमेरिकी जुमले जैसा ही अक्खड़पन है कि: ‘‘करेंसी हमारी हो सकती है लेकिन यह समस्या आपकी है’’।
इस समस्या के केंद्र में संवैधानिक प्रावधान हैं जिनके कारण बैंकों का स्वास्थ्य केंद्र की चिंता का विषय है जबकि किसानों का स्वास्थ्य राज्यों की चिंता का विषय है। उत्तरदायित्व का यह बंटवारा इस लिहाज से गैर-बराबरी का है कि अगर राज्य किसानों के हितों की रक्षा करते हैं, तो वे बैंकों की भी रक्षा करते हैं। वहीं केंद्र किसानों की चिंता किए बिना भी बैंकों की रक्षा कर सकता है। फलतः गेंद हमेशा ही राज्यों के पाले में रहती है, और केंद्र चाहे तो महज हाथ बांधे खड़ा होकर देखता रह सकता है।
यह स्थिति कुल मिलाकर देश के स्वास्थ्य के लिहाज से हितकर नहीं है। केंद्र और राज्यों को चाहिए कि वे मिलकर कृषि ऋण का कोई ऐसा मॉडल तैयार करें जिससे उसमें राजनीति घुसेड़े बिना किसानों और बैंकों, दोनो की रक्षा हो सके। यही ‘सहकारी संघवाद’ का सार भी है और जिसका दावा यह सरकार भी करती है। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक कृषि ऋण माफी को सैद्धांतिक चश्मे से देखने के बजाय अधिक करुणा भरी नजर से देखने की जरूरत है।
लेखक परिचय : प्रणब सेन इंटरनॅशनल ग्रोथ सेंटर (आई.जी.सी.) इंडिया के कंट्री डायरेक्टर हैं।




 14 दिसंबर, 2018
14 दिसंबर, 2018 


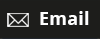

Comments will be held for moderation. Your contact information will not be made public.