रांची विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर ज्यां द्रेज़ ने भारत में सामाजिक सुरक्षा के व्यापक संदर्भ में ‘न्याय’ की भूमिका पर चर्चा की है और इस योजना के लिए कुछ संभावित सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं।
‘न्याय’ के लिए यह खौफनाक लेकिन मुमकिन परिदृश्य इस प्रकार है। इस वर्ष केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गंठबंधन की सरकार बनने के तत्काल बाद एक समिति से सबसे गरीब 20 प्रतिशत परिवारों की पहचान करने के तरीके सुझाने के लिए कहा जाएगा ताकि उन्हें 6,000 रु. प्रति माह दिए जा सकें। समिति परिवार की विशेषताओं, या संभवतः समावेश और बहिष्करण (इनक्लूजन एंड एक्सक्लूजन) संबंधी मापदंडों के कुछ संयोजनों के आधार पर किसी प्रकार की स्कोरिंग प्रणाली की सलाह देगी। उसके क्रियान्वयन के लिए 2021 की जनगणना के तत्काल बाद सामाजिक-आर्थिक जनगणना (सोसिओ-इकनॉमिक सेन्सस, एसईसी) की जाएगी – काफी कुछ उसी तरह जैसे 2011 में सामाजिक-आर्थिक एवं जाति-आधारित जनगणना (सोसिओ-इकनॉमिक एंड कास्ट सेन्सस, एसईसीसी) की गई थी, लेकिन उसमें से ‘‘जाति’’ को विवेकपूर्ण ढंग से हटाकर क्योंकि पिछली बार उससे कुछ भी निकलकर नहीं आया था। पूरे अभ्यास से परिवारों का एक नया वर्ग बनेगा जिसे मोटे तौर पर न्यूनतम मजदूरी पर मिलने वाले पूर्णकालिक रोजगार के समकक्ष मासिक भत्ता दिया जाएगा।1 उनमें से कुछ तो अत्यंत असुरक्षित समूहों से होंगे लेकिन पहचान के इस अभ्यास की अविश्वसनीय प्रकृति के कारण अन्य लोग उससे नहीं होंगे। इस कारण से अनेक गरीब परिवार छूट जाएंगे। असंतोष फैलेगा, तनाव भड़केगा, और पूरी योजना को संपूर्ण अन्याय माना जाएगा – ‘न्याय’ के बजाय ‘अन्याय’। इस बीच मुद्रास्फीति बढ़ेगी क्योंकि सरकार के पास न्याय के वित्तपोषण के लिए धनी लोगों के ऊपर कर लगाने का साहस नहीं होगा और वह घाटे के जरिए वित्तपोषण (डेफिसिट फाइनांसिंग) का सहारा लेगी। पांच वर्ष के बाद, 2024 में होने वाले अगले चुनाव में कांग्रेस इस अव्यवस्था की कीमत चुकाएगी।
निस्संदेह, यही एकमात्र संभव परिदृश्य नहीं है। और इस निराशाजनक परिदृश्य में भी काफी गरीब लोग बेहतर और अधिक सुरक्षित जिंदगी जी सकेंगे। अगर मैं इसे सामने लाता हूं तो इसलिए कि इस तथ्य को स्पष्ट किया जा सके कि न्याय के संचालन संबंधी पक्ष कोई आकस्मिक मामला नहीं है जैसा कि इसके कुछ समर्थक सुझाव देते दिखते हैं। संचालन संबंधी मुद्दों पर परियोजना या तो टिकी रह सकती है या ढह सकती है।
मैं एक अन्य मुद्दे पर भी ध्यान आकर्षित कर रहा हूं जिस पर अभी तक बहुत कम ध्यान दिया गया है। वह है न्याय का संभावित ‘‘भेदभाव’’। यह चिंता अपेक्षाकृत कम कवरेज (आबादी का 20 प्रतिशत) और बड़े लाभ के मेल से पैदा होती है – वह लाभ जो अभी किसी भी योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले लाभों से कई गुना अधिक है। उदाहरण के लिए, मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत पूरे 100 दिन काम पाने वाला भाग्यशाली परिवार पूरे साल में लगभग 20,000 रु. कमाएगा जो न्याय के तहत वादा की गई 72,000 रु. की वार्षिक रकम के एक-चौथाई से थोड़ा ही अधिक है।2 यह सुनने में बुरा लग सकता है कि अपेक्षाकृत गरीब राज्यों में 6,000 रु. अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों का – जैसे कि चौकीदारों का या घरेलू मजदूरों का मासिक वेतन होता है। इस तरह के काम के लिए लोग संघर्ष करते हैं, रिश्वत देते हैं और लड़ते हैं। आशंका है कि बिना शर्त 6,000 रु. मासिक भत्ता देने के लिए 20 प्रतिशत परिवारों को चुनना उथल-पुथल भरा और भेदभाव वाला अभ्यास होगा।
इस पोस्ट में बजट संबंधी मामलों को दरकिनार करके मैं न्याय के कुछ परीक्षात्मक (टेंटेटिव) सिद्धांत प्रस्तावित करूंगा ताकि इस महत्वपूर्ण विषय पर बहस का विस्तार हो सके। उसके पहले, न्याय को भारत में सामाजिक सुरक्षा के व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखना उपयोगी होगा।
न्याय की भूमिका
सतही तौर पर भारत में पहले से ही सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का बुनियादी आधार मौजूद है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) 67 प्रतिशत आबादी को कुछ खाद्य और आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराती है। मनरेगा हर ग्रामीण परिवार को स्थानीय सार्वजनिक कार्यों में साल में 100 दिनों तक बुनियादी मजदूरी पाने का अवसर उपलब्ध कराता है। बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन लागू हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रति बच्चा 6,000 रु. मातृत्व लाभ पाना सभी भारतीय महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार है। मध्याह्न भोजन योजना और समेकित बाल विकास सेवा (आइसीडीएस) के तहत अधिकांश बच्चों को पूरक पोषाहार और स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। शिक्षाधिकार अधिनियम (राइट टू एजुकेशन एक्ट) के तहत प्रारंभिक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य है। और कम से कम कुछ हद तक मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं भी सभी लोगों की पहुंच में हैं जिसके पूरक के बतौर हाल में आयुष्मान भारत योजना के तहत आबादी के लगभग 40 प्रतिशत हिस्से के लिए स्वास्थ्य बीमा दिया गया है।
संयोग से, इनमें से अधिकांश प्रावधान अपेक्षाकृत नए हैं, और उनमें से अधिकांश को चुनावी राजनीति से संबंधित युद्धों के बाद नहीं, तो अवश्य ही गंभीर बहस के बाद कार्यरूप दिया गया है। लेकिन यह अलग मामला है।
वास्तव में यह सुरक्षा संजाल (सेफिटी नेट) अभी भी त्रुटियों से मुक्त नहीं है। हाल के वर्षों में काफी सुधार के बावजूद जन वितरण प्रणाली में रिसाव और बहिष्करण (एक्सक्लूजन) संबंधी त्रुटियों की आशंका बनी रहती है। मनरेगा के तहत रोजगार औपचारिक आवेदन देने वाले लोगों के लिए भी ‘‘गांरटीशुदा’’ होने से बहुत दूर है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कवरेज के मामले में अभी भी अनेक राज्यों में बहुत गड़बड़ी है। मातृत्व लाभों को प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अवैध ढंग से पहले जीवित बच्चे तक सीमित कर दिया गया है। इसके अलावा, ये सभी कम लाभ वाली योजनाएं हैं: अनेक राज्यों में मनरेगा के तहत मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी से कम हैं, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के लाभों को अवैध तरीके से घटाकर 5,000 रु. प्रति बच्चा कर दिया गया है, सामाजिक सुरक्षा पेंशनों में केंद्र सरकार का योगदान पिछले 12 वर्षों से भी अधिक समय से महज 200 रु. प्रति माह पर रुका हुआ है, इत्यादि-इत्यादि।
इस पृष्ठभूमि में कमियों को दूर करने और लाभों को बढ़ाने के लिए न्याय के वादे पर गंभीरता से विचार जरूरी है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वर्ष 2004 में डॉ. मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी ने विचार शुरू किया था कि शासक दल अपने चुनावी वादों को पूरा करेंगे – या कम से कम पूरा करने का प्रयास करेंगे (अन्यथा मनरेगा अस्तित्व में आया ही नहीं होता)। निस्संदेह, कांग्रेस पार्टी अगली सरकार का नेतृत्व कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती है। लेकिन अगर वह करती है, तो इस बात की संभावना है कि न्याय को कार्यरूप देने के गंभीर प्रयास किए जाएंगे।
जैसा कि कहा गया है, न्याय अवसर और खतरा, दोनो है। भारतीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अन्य आधारों से जुड़ कर, सुनियोजित न्याय योजना प्रगति की दिशा में एक बड़ी छलांग हो सकती है। लेकिन बिना कोई बेहतर विकल्प सामने लाए, न्याय अगर सामाजिक सुरक्षा के वर्तमान आधारों को हटा दे या कमजोर कर दे, तो यह आक्रामक और लापरवाह कदम में भी बदल सकता है।
दस सुझाव
अब मुझे न्याय के लिए कुछ बुनियादी सिद्धांत प्रस्तावित करने दें। उनमें से अनेक भारत में अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, खास कर मनरेगा, जन वितरण प्रणाली, और सामाजिक सुरक्षा पेंशनों से जुड़े हुए हाल के अनुभवों से प्रेरित हैं।3 सुविधा के लिए मैं निर्देशात्मक लहजे का उपयोग करूंगा लेकिन मेरा इरादा चर्चा के लिए कुछ विचार सामने लाना भर है।
सर्वप्रथम, न्याय को सर्वाधिक पहचान उसी रूप में मिल रही है जो कि वह है – एक विशाल पेंशन योजना। आरंभिक विचार परिवार के आधार पर न्यूनतम आय और वास्तविक आय के बीच अंतर की रकम देकर न्यूनतम आय राहुल गांधी के अनुसार 12,000 रु. प्रति माह) की गारंटी करना था। हालांकि यह ‘‘टॉप-अप’’ दृष्टिकोण अव्यवहारिक है। 25 मार्च 2019 को इसकी जगह ‘‘फ्लैट रेट’’ वाले दृष्टिकोण ने ले ली जिसमें सभी प्राप्तकर्ताओं को बिना शर्त 6,000 रु. मासिक लाभ मिलेगा। उस स्थिति में ‘पेंशन’ को काम करने में अक्षम लोगों तक सीमित होने के अर्थ में न लेकर, मूल आय संबंधी भत्ता के व्यापक अर्थ में लेकर न्याय को पेंशन योजना के बतौर देखा जा सकता है। जब तक कोई विश्वसनीय व्यवस्था नहीं तैयार की जाती है जो सुनिश्चित करे कि कम आय वाले अधिकांश परिवार इस पेंशन योजना के लाभ पाने में सक्षम होंगे, तब तक ‘आय की गारंटी’ शब्द भ्रम पैदा करेंगे।
दूसरे, ‘6x20’ फार्मूला (20 प्रतिशत आबादी के लिए 6,000 रु. मासिक) को अटल आदेश नहीं समझकर इस पेंशन योजना के लिए किए जा रहे संकल्प का बेंचमार्क समझा जाना चाहिए। अगर मोटे तौर पर इसके समकक्ष लेकिन अधिक प्रभावी योजना संभव हो, तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। यहां असल में ‘6x20’ फॉर्मूला के अनेक संस्करणों की तलाश का मामला बनता है।
तीसरे, पारिवारिक पेंशनों के बजाय या उसके साथ-साथ व्यक्तिगत पेंशनों की संभावना पर भी विचार किया जाना चाहिए। जैसी स्थिति है उसमें न्याय के तहत 6,000 रु. प्रति माह पारिवारिक पेंशन देना शामिल है। पांच व्यक्ति का परिवार मानकर चलने पर यह प्रति व्यक्ति के लिहाज से औसतन 1,200 रु. प्रति माह होता है। आरंभिक बेंचमार्क के बतौर व्यक्तिगत पेंशनों को 1,200 रु. प्रति माह किया जा सकता है। समान बजट के साथ न्याय के तहत 5 करोड़ परिवारों को 6,000 रु. प्रति माह पारिवारिक पेंशन, या 25 करोड़ व्यक्तियों को 1,200 रु. प्रति माह व्यक्तिगत पेंशन दिया जा सकता है, या व्यक्तियों और परिवारों का कोई और भी संयोजन हो सकता है जो आबादी के 20 प्रतिशत हिस्से को कवर करे। इससे 6x20 फॉर्मूला की सख्ती से हटने में मदद मिलेगी। सिद्धांत रूप में विभिन्न प्रकार के परिवारों या व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार की पेंशन दरों पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि ऐसा करने के लिए ‘किस’ (“कीप इट सिंपल, स्वीटी” – “इसे सरल रखो प्रिय”) सिद्धांत को स्मरण में रखना जरूरी होगा। ऐसा इसलिए कि इस प्रकार की योजनाओं की सफलता काफी हद तक लोगों द्वारा नियमों (पात्रता के मानदंडों, आवेदन की प्रक्रिया, लाभ का स्तर, आदि) की समझ पर निर्भर करती है।
चौथे, न्याय के पेंशनों पर पहला दावा बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग लोगों का होना चाहिए। गरीब परिवारों में ही नहीं, दूसरे परिवारों में भी इन लोगों द्वारा बहुत वंचित जिंदगी जीने की आशंका रहती है। भारत में उनके लिए पहले से ही पेंशन योजना है – राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (नैशनल सोसिअल असिस्टेंस प्रोग्राम)। हालांकि जैसा पहले भी कहा गया है इन पेंशनों में केंद्र सरकार का योगदान अत्यंत कम है। अनेक राज्य अपने कोष से इसमें कुछ रकम मिलाते हैं लेकिन संयुक्त रकम भी कम ही रहती है। इसके अलावा, इस कार्यक्रम के तहत सिर्फ 3.3 करोड़ पेंशनधारी हैं जो रेफरेंस ग्रुप के महज एक-चौथाई हैं।4 न्याय के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन को यूनिवर्सल (सर्वभौमिक) बनाया जा सकता है और उसकी रकम बढ़ाकर 1,200 रु. प्रति माह कर दी जा सकती है। राज्य द्वारा दी जाने वाली रकम इससे अलग होगी। संभवतः कवरेज का ‘अर्ध-सर्वभौमिक’ करना बेहतर होगा: कुछ अच्छी तरह से निर्धारित मापदंडों के आधार पर बहिष्करण (एक्सक्लूजन) की शर्त के साथ सर्वभौमिक।5 ऐसा अपेक्षाकृत आसानी से और तेजी से किया जा सकता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का अच्छा रिकॉर्ड रहा है। यह मामला काफी हद तक इस योजना के विस्तार का है।
पांचवें, इसी तर्ज पर न्याय के तहत सभी गर्भवती महिलाओं के लिए (औपचारिक क्षेत्र से मातृत्व लाभ ले रही महिलाओं को छोड़कर) 6 या यहां तक कि 12 महीनों के लिए भी 1,200 रु. प्रति माह की दर से मातृत्व लाभ बढ़ाया जा सकता है। निस्संदेह, यहां सवाल खड़ा होगा कि इससे निम्न प्रजनन दरों के लिए चलने वाले अभियान को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन प्रजनन दरों में लगातार गिरावट आ रही है और असल में हालिया अनुमानों के एक सरल प्रोजेक्शन से पता चलता है कि भारत में यह प्रति महिला 2.1 बच्चा के प्रतिस्थापन दर पर या उसके लगभग नजदीक पहुंच चुका है। प्रजनन दर में गिरावट में थोड़ी कमी आती भी है तो सभी माताओं और बच्चों की खैरियत और अधिकारों की रक्षा की तुलना में यह संभवतः चिंता की कोई बड़ी बात नहीं होगी। तमिलनाडु जैसे राज्य यहां प्रस्तावित लाभ से अधिक लाभ पहले से ही दे रहे हैं और वहां प्रजनन दर बढ़ने की कोई सूचना नहीं मिली है।
छठे, न्याय के तहत विशेषतः आदिम जनजाति, घूमंतू जनजातियों, और सिर पर मैला ढोने वाले लोगों जैसे कुछ अत्यंत असुरक्षित समूहों के स्वतः समावेश का प्रावधान होना चाहिए। ये समूह सदियों से सामाजिक रूप से हाशिए पर धकेले जाने का भारी बोझ ढोते रहे हैं और अत्यंत गरीबी का जीवन जीते हैं। जनगणना या दूसरी चीजों के जरिए वे पहले से ही काफी हद तक चिन्हित हैं। उनके मामले में शायद बहिष्करण का कोई मापदंड नहीं होना चाहिए। पात्रता की शर्तों में थोड़ी भी जटिलता उनके लिए बड़ी बाधा बन सकती है। झारखंड में पहले से ही आदिम जनजाति के लिए एक पेंशन योजना चल रही है जिससे उन्हें काफी मदद मिलती दिखती है (ड्रेज़ 2018ए; सोमांची, शीघ्र प्रकाश्य)। सिर पर मैला ढोने वालों का पुनर्वास एक अनसुलझी चुनौती है जिससे भारत दशकों से परेशान रहा है। न्याय आखिर कार उस सीमा को पार करने का मौका हो सकता है।
सातवें, न्याय के पेंशन के एक उचित अनुपात का आबंटन ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के विवेकाधीन किया जा सकता है। गरीब परिवारों की केंद्रीकृत पहचान में बहिष्करण संबंधी काफी त्रुटियां होनी ही हैं। साथ ही, किसी परिवार की आर्थिक स्थिति समय के साथ बदलती रहती है, और केंद्रीकृत डेटाबेस को इन बदलावों के अनुरूप अपडेट करते रहना मुश्किल है। ग्राम समुदायों में यह जानने का रुझान रहता है कि उनके पास-पड़ोस में कौन परिवार या व्यक्ति सबसे गरीब है। निस्संदेह, समुदाय के जरिए पहचान की अपनी समस्याएं हैं जिसमें भ्रष्टाचार और विवाद की आशंका भी शामिल है। न्याय के सारे या अधिकांश पेंशनों का आबंटन ग्राम पंचायतों या ग्राम सभाओं के विवेक पर छोड़ देना संभवतः गलत होगा (हालांकि ग्राम पंचायत बुजुर्ग और गर्भवती महिला जैसी पूर्व-निर्धारित श्रेणियों की पहचान में मदद कर सकते हैं)। लेकिन बहिष्करण संबंधी त्रुटियों में कमी के लिए न्याय पेंशन के एक छोटे हिस्से को ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के विवेकाधीन रखने का मामला तो बनता ही है। इससे किसी परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य की अचानक मृत्यु जैसी आकस्मिक स्थितियों के मामले में कुछ सुरक्षा (इनस्योरेंस) उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।
आठवें, ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय के पेंशनों का भारी संकेंद्रण होना चाहिए। कारण यह है कि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में जीवनदशा और आर्थिक असुरक्षा की स्थिति आम तौर पर बहुत खराब है। प्रति व्यक्ति व्यय पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के आंकड़ों से हमेशा इसका पता नहीं चलता है। निस्संदेह, गरीबी के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आधारित कुछ अनुमानों के अनुसार कई राज्यों में शहरी गरीबी का स्तर भी ग्रामीण गरीबी जितना ही ऊंचा है।6 हालांकि शहरी और ग्रामीण गरीबी की तुलना में मूल्य सूचकांक (प्राइस इंडेक्स) संबंधी समस्याओं समेत अनेक समस्याओं जैसे रहने के मौहाल, सामाजिक अधिसंरचना, सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता आदि मामलों में अंतरों का लेखा-जोखा लेने में कठिनाइयों के सामने आने का भय है। गौरतलब है कि ‘‘बहुआयामी गरीबी’’ (मल्टीडिमेन्शनल पावर्टी) के अनुमान जीवनदशा के प्रत्यक्ष मूल्यांकन पर आधारित हैं जो गांवों और शहरों के बीच अधिक तीक्ष्ण अंतर (कंट्रास्ट) का संकेत देते हैं। जैसे 2015-16 में बहुआयामी गरीबी वाले लोगों की संख्या ग्रामीण भारत में 36.5 प्रतिशत थी जबकि शहरी भारत में महज 9 प्रतिशत थी।7 वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के साथ इन आंकड़ों को मिलाकर देखने पर यह अर्थ निकलता है कि भारत में 90 प्रतिशत गरीब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। शहरी क्षेत्रों में न्याय के पेंशन मुख्यतः मलिन बस्तियों में रहने वाले, बेघर, और सिर पर मैला ढोने वाले जैसे अन्य सुनिर्धारित असुरक्षित समूहों पर केंद्रित होने चाहिए।
नवें, न्याय का आरंभ एक योजना के बतौर होना चाहिए और उसके बाद अगर यह अच्छी तरह काम करे, तो कानूनी ढांचे की ओर बढ़ना चाहिए। कानूनी ढांचे के बिना योजना अल्पजीवी साबित हो सकती है। जो व्यवस्था गरीब लोगों को बहुत कम अधिकार देती है, उसमें अपना उचित हक पाने में उन्हें कानूनी हकदारियों से मदद मिलती है। कानून में न्याय पेंशन की रकम के कीमतों के स्तर पर सूचीकरण (इंडेक्सेशन) के लिए प्रावधान होना चाहिए या उससे भी बेहतर होगा कि समय के साथ न्याय पेंशन के वास्तविक मूल्य में कुछ वृद्धि होती रहे।8 ऐसा नहीं होने पर सरकार के लिए आसान होगा कि वह नकद अंतरणों के वास्तविक मूल्य में कमी होती रहने दे जैसा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता कार्यक्रम के पेंशनों के मामले में हुआ है।
और दसवें, नकद अंतरण की प्रौद्योगिकी पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है। सरकार द्वारा किए गए वित्तीय समावेश के लंबे-चौड़े दावों के बावजूद भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी नकद अंतरण के लिए विश्वसनीय और उपभोक्ता के अनुकूल अधिसंरचना की कमी है। पिछले कुछ वर्षों में जन वितरण प्रणाली के खाद्य राशनों को नकद अंतरण के साथ बदलने के लिए अनेक प्रयासों के बावजूद अच्छे परिणाम नहीं आए हैं, जिसका आंशिक कारण भुगतान संबंधी प्रौद्योगिकियों का दोषपूर्ण होना है। झारखंड में ‘खाद्य सुरक्षा हेतु प्रत्यक्ष लाभांतरण’ प्रयोग एक प्रमुख उदाहरण है (ड्रेज़ 2018बी)। यहां तक कि पुदुचेरी और चंडीगढ़ जैसी अनुकूल स्थिति वाली जगहों पर भी ऐसे पायलट-प्रयोगों में गंभीर समस्याएं पैदा हो गई हैं (जे-पाल 2016; मुरलीधरन एवं अन्य 2017)। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम खास तौर पर समस्यापूर्ण प्रौद्योगिकी है (धोराजीवाला एवं अन्य 2019)। आधार-एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में भी असफलता की दरें काफी ऊंची रही हैं (बालासुब्रामनियन एवं अन्य 2019)। प्रौद्योगिक गड़बड़ी जो बाकि जोखिमों को और भी बढ़ादे, वैसी आखिरी चीज़ है जिसकी न्याय को इस समय ज़रुरत है।
ये 10 सुझाव न्याय की किसी स्पष्ट योजना के समान नहीं हैं। हालांकि ये चीजें कुछ वर्षों के अंदर न्याय के लगभग आधे वादे को काफी सुरक्षित और आकर्षक ढंग से निभाना मुमकिन बना देंगी। मेरे दिमाग में यह बात है कि मैंने जिन आरंभिक लक्ष्य समूहों (बुजुर्ग, विधवा, गर्भवती महिला, आदिम जनजाति, आदि) का प्रस्ताव दिया है उनमें आबादी के 10-12 प्रतिशत हिस्से का समावेश होने की संभावना है जो न्याय के 20 प्रतिशत प्रस्तावित कवरेज का लगभग आधा है।9 'पहले कदम' के बतौर उनको कवर करने से भेदभाव से बचने और निस्संदेह न्याय के लिए एक व्यापक दल तैयार करने का भारी लाभ मिलेगा। वृद्धावस्था पेंशन और मातृत्व लाभों के संभावित प्राप्तकर्ताओं के रूप में अधिकांश घरों का इसमें हित जुड़ जाएगा। इसके अलावा, कार्यसंचालन संबंधी चुनौतियां काफी कम हो जाएंगी क्योंकि यह मुख्यतः पहले से ही चल रही योजनाओं के विस्तार और समेकन का मामला है। राजनीतिक रूप से देखें, तो इस पहले कदम से लोगों में उत्साह पैदा होने की संभावना है, और पूरी परियोजना की सफलता के लिए यह ज़रूरी है।
अभी न्याय के शेष आधे हिस्से को मैं पाठकों और भावी टिप्पणीकारों की कल्पना पर छोड़ता हूं। मेरा यह कहना नहीं है कि अगले कदम के बारे में स्पष्ट हुए बगैर ही पहला कदम उठा लिया जाना चाहिए। न्याय के आरंभ के पहले इसका शुरुआत से अंत तक का रोडमैप तैयार होना ज़रूरी है। हालांकि संभावना है कि इसके लिए एक निर्धारित समय के लिए सहभागी परामर्श प्रक्रिया की जरूरत होगी जो अर्थशास्त्रियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। 6x20 फार्मूला को लागू करने के लिए किसी विशेषज्ञ समिति के गठन से काम नहीं चलेगा।
नोट्स:
- मैं यहां कृषि श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी के बारे में बात कर रहा हूं। कृषि श्रमिक के लिए राज्यों में जनसंख्या-भारित (पोपुलेशन-वेटेड) औसत न्यूनतम मजदूरी लगभग 250 रु. प्रतिदिन है। महीने में 25 कार्यदिवस मानकर चलने पर उस दर पर पूर्णकालिक रोजगार से 6,250 रु. प्रति माह प्राप्त होंगे।
- वर्ष 2019-20 में मनरेगा के तहत मजदूरी की दरों का पॉपुलेशन-वेटेड औसत 200 रु. प्रतिदिन से कुछ कम है।
- देखें द्रेज (2017), द्रेज एवं खेड़ा (2017), और वहां उद्धृत साहित्य। न्याय पर कुछ संबंधित विचार के लिए देखें द्रेज (2019), खेड़ा (2019) और मंडल (2019)। वित्तपोषण के मुद्दे पर, जिस पर यहां चर्चा नहीं की गई है, एक यथार्थपूर्ण बात यह सामने लाई गई है कि संपन्न लोगों को इसका भार वहन करना चाहिए (भारती एवं चांसेल, 2019)। निस्संदेह, भारत में संपन्न लोगों को असीम प्यार-दुलार मिलता रहा है। भारत में कोई उत्तराधिकार कर नहीं है, संपत्ति कर नहीं है, करों के मामले में ढेर सारी छूटें मिलती हैं, सभी प्रकार की प्रतिगामी सब्सिडी हैं, और सबसे ऊपर महज 30 प्रतिशत सीमांत आय कर है (जबकि अधिकांश पश्चिमी देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित उत्तरी अमेरिकी देशों में यह 40 से 60 प्रतिशत है)।
- 25 अप्रैल 2019 को http://nsap.nic.in/ से प्राप्त आधिकारिक आंकड़े। इसी स्रोत के अनुसार, अन्य 45 लाख लोगों को राज्यों की पेंशन योजनाओं के तहत कवर किया गया है।
- समावेश और बहिष्करण मापदंडों के अन्य संभावित उपयोगों के साथ इस दृष्टिकोण पर ड्रेज़ एवं खेड़ा (2010) द्वारा चर्चा की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में ड्रेज़ एवं अन्य (2019) भी देखें। आरंभिक अनुच्छेद की संभावित गलत समझ से बचने के लिए, मैं समावेश एवं बहिष्करण मापदंड को लागू करने के मकसद से सामाजिक-आर्थिक गणना की संभावित उपयोगिता पर कोई विवाद नहीं खड़ा कर रहा हूं।
- रंगराजन विशेषज्ञ समूह द्वारा गणना किये गए 2011-12 के गरीबी अनुमानों की यह महत्वपूर्ण विशेषता है। वस्तुतः, इन अनुमानों के अनुसार 2011-12 में भारत के आधे प्रमुख राज्यों में शहरी गरीबी का स्तर ग्रामीण गरीबी से ऊंचा था। वर्ष 2004-05 में लकड़ावाला समिति की रिपोर्ट पर आधारित गरीबी के अनुमानों में भी यही पैटर्न दिखता है। ये अनुमान भी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित थे। अधिक जानकारी के लिए देखें डीटन एवं ड्रेज़ (2014), और रंगराजन एवं महेंद्र देव (2015)।
- सबीना अलकायर द्वारा कृपापूर्वक उपलब्ध कराए गए ऑक्सफोर्ड पोवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के अप्रकाशित अनुमान। वर्ष 2011-12 के अनुमानों से भी यही निष्कर्ष निकलते हैं: भारत के लगभग 90 प्रतिशत गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। देखें OPHI (2019) ।
- ऐसा, उदाहरण के लिए, नॉमिनल जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) पर पेंशन की रकम की इंडेक्सिंग करके किया जा सकता है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआइ) के संदर्भ में एसे ही एक प्रस्ताव के लिए, देखें रे (2016)।
- इस सूची में बड़े समूह विधवाओं और बुजुर्गों के हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इनका आबादी में लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा है। लेकिन अगर (मलिन-बस्तियों आदि को छोड़कर) शहरी क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया जाय, तो संभावना है कि यह आबादी 8 प्रतिशत के आसपास होगी। बहिष्करण के मापदंडों को लागू करने पर यह 8 प्रतिशत आबादी भी अधिक ही है। प्रति 1,000 पर 20 जन्म की जन्म-दर, और सभी गर्भवती महिलाओं के लिए 12 महीनों के लिए व्यक्तिगत न्याय पेंशन के जरिए 2 प्रतिशत और आबादी न्याय के तहत आ जाएगी। लेकिन यह अनुपात भी अधिक है क्योंकि अनेक महिलाओं को औपचारिक क्षेत्र में पहले से ही मातृत्व लाभ मिलता है (और जन्म-दर में भी लगातार गिरावट आ रही है)। इस पोस्ट में जिन अन्य प्राथमिकता समूहों का उल्लेख किया गया है, उनकी आबादी 2 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना नहीं है।




 14 मई, 2019
14 मई, 2019 


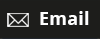

Comments will be held for moderation. Your contact information will not be made public.