
मजदूर, कारीगर, छोटे किसान और अन्य साधनहीन लोग पहले की तुलना में आज अधिक अपमानजनक जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। कोविड-19, एक महामारी, जिसने समस्त दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस लेख में प्रेमकुमार मणि ने इस बात पर चर्चा की है कि आखिर हमें अर्थ-केंद्रित संस्कृति से खुशहाली-केंद्रित संस्कृति की ओर प्रस्थान क्यों करना होगा।
कोविड-19, एक महामारी, जिसने समस्त दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पूरी दुनिया लॉक डाउन में है। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक 45 लाख से भी ज्यादा लोग आक्रांत हैं और करीब ढाई लाख लोग मर चुके हैं। यूरोप और अमेरिका तो पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, और भारत में यह बड़ी तेजी के साथ यह फैलता जा रहा है। दो हज़ार नौ सौ से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, और उसके तीस गुना से अधिक इस व्याधि से ग्रस्त हैं। स्थिति भयावह है। लोग भय से घरों में दुबके हैं। लेकिन यह कोई इलाज तो नहीं है।
बीमारियां आती-जाती रहती हैं और आती-जाती रहेंगी। इस महामारी को देख कर मेरे मन में यह विचार आ रहा है कि हरप्पा-मोइनजोदडो और बेबीलोनिया की नगर सभ्यताएं ऐसी ही किसी संक्रामक बीमारी से तो तबाह नहीं हुईं होंगी? हरप्पा के विनाश पर विचार करते हुए कतिपय इतिहासकारों ने ऐसे मत व्यक्त किये हैं। इतने विशाल क्षेत्र में फैली उत्कृष्ट-सी नगर सभ्यता ख़त्म हो गयी। लोग भाग कर मैदानी इलाकों और पहाड़ों पर चले गए। एक लम्बे समय तक नगर सभ्यता आतंक की सभ्यता बनी रही। इन सब की एक लम्बी कहानी है।
इस महामारी ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। रेनेसां और इनलाइटमेन्ट युग की वैचारिक निष्पत्तियाँ, आद्योगिक क्रांति एवं पूँजी; और सब से बढ़ कर विकास केंद्रित समाज के तमाम पहलुओं को इस महामारी ने एक झटके में ध्वस्त कर दिया है। समाजवादी सरकारों ने भी मौलिक रूप से कोई अलग दृष्टि नहीं दी थी। पूंजीवादी प्रवृति यदि पूँजी पर कुछ सीमित लोगों का अधिकार घोषित करता है, तो समाजवादी प्रवृति सरकारों का अधिकार घोषित करती है, जिस पर थोड़े से चालाक लोग कब्ज़ा जमाये होते हैं। चीन में यही हो रहा है। वहां लाल झंडे के नीचे पूंजीवाद अंगड़ाइयां ले रहा है। वाशिंगटन और बीजिंग के पूंजीवाद में कौन ज्यादा अमानवीय है, कहना मुश्किल है।
मेहनतकश तबकों की चिंता किसी को नहीं है। इस वक़्त की दुनिया जितनी अधिक गैरबराबरी पर टिकी है, इतिहास के किसी दौर में नहीं थी। मजदूर, कारीगर, छोटे किसान और अन्य साधनहीन लोग पहले की तुलना में आज अधिक अपमानजनक जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। लेकिन क्या किया जाय! सच्चाई यही है कि वे उत्पीड़ित हैं और आह भी नहीं बोल सकते। उनके लिए दूसरे लोग पहले बोला करते थे। आज उनके लिए, लोगों द्वारा कभी-कभार चालाकी भरे बयान भले निकल जाएँ, परंतु सड़कों पर कोई नहीं उतरने वाला।
तबाही के इस मोड़ पर हम आखिर कैसे पहुँचे? मीडिया में एक खबर देखी कि प्रतिदिन अड़तीस हजार करोड़ रुपये का नुकसान केवल हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को हो रहा है। महामारी से तो कुछ हजार या लाख लोग मरेंगे। अगर अर्थव्यवस्था इसी तरह बर्बादी झेलती रही, तो एक रोज इसका मौजूदा स्वरुप स्वतः नष्ट हो जाएगा। मौजूदा स्वरुप यानि पूँजीकेंद्रित ढ़ाँचा। अधिक संभावना इस बात की है कि इस ज़माने में पूँजी, जो शक्ति का पर्याय था, विनष्ट हो जायेगा। पूँजी का मरना एक सभ्यता और संस्कृति का मरना होगा।
यह स्थिति क्यों आई? अमेरिकी फिलॉसफर नोआम चॉम्स्की ने पिछले दिनों यह बात को बड़े कायदे से रखी। हमारी सरकारों, वित्तीय संघटनों और बाज़ारों ने लाभ केंद्रित अर्थव्यवस्था विकसित की है, कल्याण केंद्रित नहीं। मुनाफे वाली ऐसी व्यवस्था यह नहीं सोचती कि जीडीपी (सक पूर्व ल घरेलू उत्पाद) और सेंसेक्स की छलांगे किस हद तक मनुष्य सापेक्ष है। लोकतंत्र ने इतना अवश्य किया है कि मनुष्यता की सीमा का परिष्कार कर दिया है। उन्नीसवीं सदी तक हम भूदासों, आदिवासियों, दलितों और इसी तरह के अन्य अनेक तबकों को मनुष्येतर मानते थे। विचारकों और लेखकों के निरंतर संघर्ष ने उन्हें मनुष्य कहलाने के घेरे में लाया। इस बीच पुरानी सामंतवादी व्यवस्था औद्योगिक उपकरणों की बदौलत पूंजीवादी व्यवस्था में बदल गयी। इस व्यवस्था ने सामंतवादी-पुरोहितवादी मान्यताओं को अपनी जरुरत के हिसाब से हटाया, इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि इसका एक प्रगतिशील चेहरा भी है। लेकिन जल्द ही यह अपने वास्तविक स्वरुप में आ गया और महसूस हुआ यह तो कुछ मामलों में पुरानी व्यवस्था से भी अधिक क्रूर है।
पुरानी व्यवस्था में अस्पताल नहीं थे तो किसी के लिए नहीं थे। फिर ऐसा जमाना आया कि अस्पताल बने और इसमें अमीर-गरीब सब जा रहे हैं। यदि जा नहीं भी रहे हैं तो जा सकते हैं की स्थिति तो अवश्य थी। स्कूलों का भी यही हाल था। आज वह स्थिति नहीं है आज कुछ लोगों के लिए बड़े और व्यवस्थित अस्पताल हैं, लेकिन वहाँ केवल अमीर जा सकते हैं। अस्पतालों में भर्ती होने की पहली शर्त बीमार होना नहीं, अमीर होना है। स्कूलों का भी यही हाल है। अभी इस महामारी की बात लीजिए, खबरों के मुताबिक अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद में से दो तिहाई अश्वेत लोग हैं। हेल्थ इंस्युरेन्स की मोटी किश्त जो नहीं दे सकते, वे मरने के लिए विवश हैं। यही लोकतंत्र की मानवीय व्यवस्था है।
भारत का इससे कहीं बुरा हाल है। नेहरू युग में देश की आर्थिक स्थिति खस्ता थी, लेकिन कुछ विचार जीवित थे। इनके सहारे हमने चेचक, मलेरिया तथा हैजा जैसी कितनी महामारियों से संघर्ष किया और जीते। आज कोरोना से हम जो आतंकित और तबाह हैं, उसका कारण यह है कि इससे जूझने के लिए हमारे पास न साधन हैं, न संकल्प और न ही कोई विचार। मुझे कुछ कहने की जरुरत नहीं होनी चाहिए। आप खुद सोचिए कि सरकारें क्या कर रही हैं। कभी ताली, कभी दीप तो कभी आसमान से फूल बरसा कर आप किसे भुलावे में रख रहे हैं। आप अपनी हार स्वीकार क्यों नहीं करते?
हमारी लोकतान्त्रिक सरकारें जो लाभ केंद्रित बजट बनती हैं, उसमे स्वास्थ्य और शिक्षा का स्थान सबसे नीचे होता है। देशों के बीच सामरिक लड़ाइयां पहले के मुकाबले कम या नगण्य होती जा रही हैं, परंतु हर देश का रक्षा बजट सबसे ऊपर होता है। इसी रक्षा बजट में राजनेताओं और उनके दलालों के हित सुरक्षित होते हैं। पुराने कुलीन तबके का एक बड़ा हिस्सा सेना में अफसर बन कर काबिज रहता है। यह किसी एक देश की नहीं, बल्कि अधिकतर देशों की कहानी है। इसके बाद सड़कें और इस तरह की जो दूसरी चीजें विकसित की जा रही हैं उनके पीछे भी लाभ और लूट का किस्सा होता है। स्कूल अस्पताल के विकास से यह संभव नहीं होता। इनके विकास से मानवीय सूचकांक में भले वृद्धि होती हैं, लेकिन जीडीपी नहीं बढ़ पाता। जिस इकॉनमी की जीडीपी बढ़ती रहती है वह हीं असली इकॉनमी होती है। इसमें लगातार लाभ का एक हिस्सा बड़े कायदे और निरंतर गति से सरकार के पास जाता रहता है। फिर सरकार उतने ही कायदे और लगभग उतनी ही गति से पूंजीपतियों के कब्जे में होती चली जाती है।
लेकिन अब जब पूँजी ही मर जाएगी तब क्या होगा? ये फैक्ट्रियां बिना मजदूरों के चल पाएँगी? कैसे चलेंगी? पूँजी पर आधारित विकास की पूरी संस्कृति पूरा तामझाम एक हीं बार में खत्म हो जायेगा। बाजार और इनकी अनुसंगी संस्थाएं लगभग ध्वस्त हो चुकी हैं। यह लोकतंत्र कब ध्वस्त हो जायेगा, कोई नहीं जानता।
ऐसे में एक नयी सभ्यता, नए धर्म, तथा नयी सोच का स्वाभाविक प्रदुर्भाव होना लाजिम है। मैं कहता रहा हूँ कि विकास की इस झूटी संस्कृति को खत्म किया जाना चाहिए। संसाधनों से ख़ुशी नहीं मिलती, और केवल उपभोग से भी ख़ुशी नहीं मिलती। खुशियां कैसे मिले इसके लिए सामाजिक दार्शनिकों को मिल-बैठ कर विमर्श करना चाहिए। हमें अर्थ-केंद्रित संस्कृति से खुशहाली-केंद्रित संस्कृति की ओर प्रस्थान करना ही होगा।
लेखक परिचय: श्री प्रेमकुमार मणि बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं।
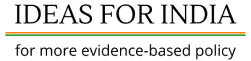

.svg)
.svg)
.svg)

.svg)



































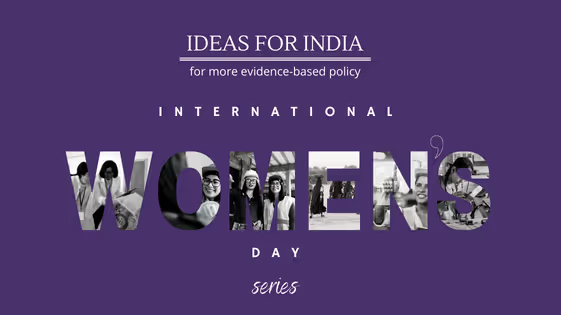



















































.svg)

.svg)
%201.svg)
.svg)
.svg)