
जलवायु पर अलग-अलग देशों की प्रतिबद्धताओं से यह साफ है कि पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के ऐसे स्तर का सामना करने वाली है जिसकी सीमा सहनीय जलवायु नुकसान पहुंचाने वाले स्तर से काफी ऊपर होगी। और आगे चल के इन नुकसानों की सबसे ज्यादा खामियाजा विकासशील देशों को हीं भुगतना पड़ेगा। इस पोस्ट में, इंगमार शूमाकर का तर्क है कि जलवायु को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान देना विकासशील देशों के हित में हीं होगा।
वर्तमान जलवायु स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस सदी के अंत तक विश्व के औसत तापमान के 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। यह स्तर 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा से काफी ज्यादा है। अर्थात पूरी दुनिया तापमान के ऐसे स्तर का सामना करने वाली है जिसकी सीमा सहनीय जलवायु नुकसान पहुंचाने वाले स्तर से काफी ऊपर होगी। इसके अलावा, जब जलवायु क्षति की बात आती है, तो विकासशील देश ऐसे देश हैं जिन्हें इन नुकसानों का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विकासशील देशों के समूह में, भारत वह देश है जिसे सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। और भारत के भीतर, समृद्ध लोगों की तुलना में गरीब आबादी ज्यादा प्रभावित होंगे। नतीजतन, इससे न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश के भीतर असमानता काफी बढ़ेगी, बल्कि यह आर्थिक विकास में गिरावट, जलवायु प्रवासन में वृद्धि, ऊंचे ऋण, मानव स्वास्थ्य और राजनीतिक स्थिरता में गिरावट को भी बढ़ावा देगा।
ऐसी संभावनाओं को देखते हुए, विकासशील देशों को क्या करना चाहिए? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया में दो मुख्य नीतियां उपलब्ध हैं। एक उत्सर्जन को कम करने के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का उपशमन करना है और दूसरा अनुकूलन के माध्यम से जलवायु के नुकसान का उपशमन करना है। हालांकि, दोनों नीतियों की अपनी खूबियां और समस्याएं हैं।
जलवायु परिवर्तन का उपशमन
यदि दुनिया जलवायु परिवर्तन को सीमित करना चाहती है तो एक ही विकल्प उपलब्ध है और वह कार्बन उत्सर्जन पर महत्वपूर्ण रुप से रोक लगाना है। हालांकि, इसे हासिल करना काफी कठिन साबित हुआ है। दुनिया के तमाम देशों ने 1995 में बर्लिन में पहले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी) के बाद से कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर आम सहमति बनाने की कोशिश की है। हालांकि, यह सर्वविदित है कि उत्सर्जन को कम करने का सबसे कुशल तरीका कार्बन बाजार का निर्माण है जो या तो कार्बन की एक कीमत तय करके या एक कैप-एंड-ट्रेड1 दृष्टिकोण पेश करके किया जा सकता है, लेकिन राजनेताओं ने इक्विटी चिंताओं के महत्व पर जोर दिया है। उदाहरण के लिए, एक चिंता यह है कि क्या विकासशील देशों को विकसित देशों की तुलना में उत्सर्जन कम करने के संदर्भ में कम बढ़ाएँ होनी चाहिए, ताकि वे भी समृद्ध राष्ट्रों के आर्थिक स्तर की बराबरी कर सकें। दूसरी चिंता यह है कि विकसित देशों को उत्सर्जन में कटौती का सबसे बड़ा बोझ उठाना चाहिए क्योंकि उनके इतिहास एवं संचित उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन के मुख्य चालक रहे हैं।
हालांकि, इक्विटी चिंताओं ने बहस को काफी हद तक अव्यवस्थित कर दिया है और इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दुनिया के राष्ट्र अभी तक वैश्विक कार्बन बाजार जैसे टॉप-डाउन, सहकारी दृष्टिकोण के निर्माण के लिए आम सहमति बनाने में कामयाब नहीं रहे हैं। इसके बजाय, 2015 में पैरिस में आयोजित सीओपी-21 की बैठक में, वैश्विक सहकारी दृष्टिकोण ने एक विकेन्द्रीकृत, गैर-सहकारी रास्ता दिया गया, जहां सभी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी), यानी कि उनके संभावित उत्सर्जन में कमी को रेखांकित कर सकते हैं। इन एनडीसी की समस्या यह है कि, दक्षता और इक्विटी के अलावा, वे एक रणनीतिक पैमाना पेश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक क्षेत्र नेतृत्व की भूमिका निभाने का फैसला करता है (जैसा की जर्मनी का एनर्जिवेन्डे) और 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जितना जरुरी हो उससे भी ज्यादा अपने उत्सर्जन को कम करता है। और अगर वह क्षेत्र यह उम्मीद करता है कि अन्य सभी क्षेत्र समान रुप से काम करेंगे, तब अन्य क्षेत्र उत्सर्जन कम करने के उनके प्रयासों को सीमित कर, इससे लाभान्वित हो सकते हैं, अन्य नीतियों पर पैसा खर्च कर सकते हैं और दुनिया तब भी कुछ हद तक सुरक्षित 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य प्राप्त करेगी। इसके अलावा, जिन क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन से कुछ हद तक कम प्रभावित होने की संभावना है, वे शायद इन उत्सर्जन में कटौती में योगदान नहीं देंगे। अंत में, कुछ क्षेत्र प्रत्याशित उत्सर्जन में कटौती की घोषणा में देरी करके ‘प्रतीक्षा करने और देखने’ की रणनीति बना सकते हैं ताकि वे अन्य क्षेत्रों के प्रयासों का निरीक्षण करें और फिर अपनी बेहतर प्रतिक्रिया को चुनें।
यह कारण है कि सारे एनडीसी संयुक्त रूप में भी उत्सर्जन उतना कम नहीं कर पाए हैं जितने की ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए आवश्यकता होती है। इसके बजाय, वर्तमान एनडीसी इतने हैं जो हमें 3 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर के स्तरों की वार्मिंग के रास्ते पर ले जा रहे हैं। वार्मिंग के इन चुनौतीपूर्ण स्तरों का सामना करते हुए यह तर्क दिया जाता है कि क्षेत्रों के पास विकल्प कम हैं, इसलिए उन्हें भविष्य में होने वाली नुकसान की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
जलवायु क्षति के लिए अनुकूलन
कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने के लिए पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की कमी के कारण, आजकल हर देश जलवायु क्षति के अनुकूलन के लिए एक महत्वपूर्ण बजट समर्पित करता है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ (ईयू) के पास अनुकूलन पर 2013 की यूरोपीय संघ की रणनीति है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) अपने राष्ट्रीय अनुकूलन योजना के माध्यम से देशों का समर्थन करता है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफ़सीसीसी) के पास एक ग्रीन क्लाइमेट फंड है जिससे वह विकासशील देशों की अनुकूलन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करता है। जलवायु परिवर्तन पर अपनी राष्ट्रीय कार्य योजना में, तथा अपनी पहली एनडीसी रूपरेखा में, भारत ने विभिन्न अनुकूलन उपायों पर सबसे ज्यदा चर्चा की है। शोध-साहित्य में अनुकूलन उपायों पर विचार करने की 'जरूरत' पर जोर दिया जा रहा है और जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) द्वारा विशेष रूप से समर्थित है, जो यह तर्क देता है कि, ‘प्राकृतिक एवं मानव प्रणालियों पर जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से बनाए जलवायु नीति में विविध अनुकूलन तथा शमन क्रियाओं का पोर्टफोलियो शामिल है।’ जब सीमित शमन प्रयासों का सामना करना पड़ता है तो अनुकूलन को विकासशील देशों के लिए एक वरदान माना जाता है।
हालांकि, वैश्विक दृष्टिकोण से, अनुकूलन पर निवेश करने का कोई तुक नहीं बंता। वास्तव में, शमन के बजाय अनुकूलन के लिए ज्यादा धन का इस्तेमाल करने का मतलब कम वैश्विक कल्याण होगा। यह तर्क सरल है: अनुकूलन में निवेश किए गए पैसों से दुनिया की आबादी के केवल एक छोटे उप-समूह को लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए, एयर कंडीशनिंग स्थापित करना (भारत के कुछ क्षेत्रों में 2019 में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था) अनुकूलन का एक रूप है जो केवल एक ही परिवार को लाभ पहुंचाता है, जबकि एक बांध से उस क्षेत्र के निवासियों के बहुत छोटे समूह को लाभान्वित किया जा सकता है। इसके बजाय, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए खर्च किए गए पैसे से पूरा ग्रह प्रभावित होता है। मान लीजिए कि धरती पर प्रत्येक व्यक्ति अनुकूलन पर € 100 (€ - यूरो) खर्च करता है। यह बल्कि एक रूढ़िवादी राशि है, उदाहरण के लिए, जैसे एक एयर कंडीशनर की स्थापना में पहले से ही कई हजार यूरो खर्च होते हैं। इस अनुकूलन व्यय का वैश्विक कुल € 78000 करोड़ होगा। यह 2030 तक वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए उत्सर्जन में कमी (अनुमानित € 260-600 बिलियन) की कुल अनुमानित लागत से काफी ज्यादा है। वास्तव में, हाल के अनुमान बताते हैं कि अनुकूलन की वार्षिक लागत 2030 के बाद से € 12500-27000 करोड़ हो सकती है, और यह 2050 तक दोगुनी हो जाएगी। इस प्रकार अनुकूलन की तुलना में विश्व स्तर पर शमन करना ज्यादा किफ़ायती साबित होगा।
गौर करने पर एक और समस्या दिखाई देती है – अन्य देशों द्वारा उनके उत्सर्जन पर अंकुश लगाने का प्रयास भी जलवायु परिवर्तन की अपेक्षित लागतों पर निर्भर करता है। यदि अनुकूलन पर्याप्त रूप से प्रभावी है और क्षेत्र जलवायु परिवर्तन का अनुकूलन कर सकते हैं, तब अन्य देश भी अपने उत्सर्जन को फिर से बढ़ाने का जोखिम उठा सकते हैं, जैसा कि तब सीमांत जलवायु क्षति कम होगा। इससे उत्सर्जन में वृद्धि होगी और फिर अनुकूलन का एक दुष्चक्र चल सकता है, जिसे बाद में फिर से अनुकूलन में वृद्धि की आवश्यकता है। इसका परिणाम ना केवल जलवायु परिवर्तन में ज्यादा बदलाव के रुप में सामने आएगा बल्कि अनुकूलन की लागत में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार अनुकूलन विकल्प आसानी से विकासशील राष्ट्रों के लिए अभिशाप बन सकता है।
विकासशील देशों को क्या करना चाहिए?
वैश्विक परिप्रेक्ष्य से देखें, तो यह स्पष्ट है कि पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में, वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पर सीमित करने के लिए कार्बन उत्सर्जन को रोकना जरुरी है और इसके लिए एक समाधान समन्वित प्रयास ही है। कम अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ तथा अगर किसी व्यक्तिगत देश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, रणनीतिक पहलू एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अनुकूलन एक प्रासंगिक नीति विकल्प बन जाता है।
लेकिन अनुकूलन पर अपेक्षाएं बहुत ऊंची राखी जा सकती हैं। हाल के अनुभवजन्य साक्ष्य (हेन्सेलर और शूमाकर 2019) में पाया गया है कि जलवायु क्षति का सबसे बड़ा बोझ गरीबों पर पड़ने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है, जिसका आंकड़ों से पता चलता है कि नुकसान न केवल गरीब देशों में आर्थिक विकास को प्रभावित करता है, बल्कि उत्पादन के सभी कारकों (श्रम, पूंजी और उत्पादकता) को भी प्रभावित करता है। इससे पता चलता है कि गरीब देश जलवायु क्षति से अपनी आर्थिक गतिविधि को बचा नहीं पाए हैं। इसका एक कारण अनुकूलन के लिए पर्याप्त धन नहीं होना या जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने में परेशानी होना हो सकता है।
यह मानते हुए कि विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल होना संभव है, बजट सीमाएं एक बड़ी बाधा होगी। जैसा कि ऊपर सुझाव दिया गया है, अपेक्षित जलवायु क्षति के अनुकूल होने के लिए हर साल सैकड़ों अरब पैसों की जरुरत होगी। इस राशि को शिक्षा, बुनियादी ढांचे या स्वास्थ्य जैसे अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं से निकालना होगा, जो बदले में विकासशील देशों में विकास को घटाएगा और गरीबों के आर्थिक रूप से सममृद्ध होने या ऊर्जा संक्रमण के लिए भुगतान करना मुश्किल बनाएगा, जोकि सतत ऊर्जा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
एक और समस्या यह है कि करीब 2010 तक अमीर देश कार्बन उत्सर्जन के सबसे बड़े उत्सर्जक थे, लेकिन अब विकासशील देश हैं जो सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने में योगदान दे रहे हैं। आज की तारीख में, चीन कार्बन का सबसे बड़ा उत्सर्जक है (वैश्विक उत्सर्जन का 26%)। इसके बाद अमेरिका (13%), और फिर भारत (7%) है। और इस दिशा में विकासशील देश तेजी से पकड़ बना रहे हैं। भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 1960 में 0.12 गिगाटन से बढ़कर वर्ष 2000 में बढ़कर 1 गिगाटन हो गया था, और वर्ष 2017 में 2.45 गिगाटन पर पहुंच गया था। भारत के एनडीसी के अनुसार वह अपनी ऊर्जा की तीव्रता को कम करने की योजना बना रहा है, परंतु इसके बावजूद राष्ट्रीय उत्सर्जन अभी भी बढ़ते हीं रहेंगे।
भारत अभी भी विकसित हो रहा है, और यदि भारत, अमेरिका के वर्तमान प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के स्तर तक पहुँचना चाहता हो तो उसे अमेरिका के समान उत्सर्जन करना पड़ेगा जो भारत की वर्तमान स्थिति से 10 कारक ज्यादा है। इसका मतलब, अगर ऐसा हुआ तो केवल भारत आज के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के दो-तिहाई का उत्पादक होगा। यदि चीन इसी तरह से बढ़ता है, तो भारत और चीन अकेले आज की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा वार्षिक कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होंगे। यह कहने की जरुरत नहीं कि इससे जलवायु परिवर्तन उस स्तर पर चला जाएगा जिससे अनुकूल दुनिया शायद ना हो पाए। हालांकि, जब अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौतों और रणनीतिक बातचीत की बात आती है, कार्बन उत्सर्जन में यह वृद्धि क्षमता उन्हें ऐसे लाभ दे सकती हो जिसे विकसित राष्ट्र अनदेखा नहीं कर सकते हैं।
दूर्दर्शी सुझाव
ज्यादातर विकासशील देशों की तरह, भारत में, वर्तमान में 70% ऊर्जा जीवाश्म ईंधन (फ़ौसिल फ्युल) से आती है। भारत की राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) को देखते हुए, इस बात की संभावना कम है कि भारत अपने प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन को अमेरिका के निम्न स्तर तक बढ़ाएगा। फिर भी, अधिकांश विकासशील देशों की तरह, भविष्य में, जब तक कि कोई प्रभावशाली परिवर्तन न हो, तब तक भारत का कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ने वाला है। वर्तमान में चीन और भारत जैसे देश सबसे तेजी से विकसित हो रहे हैं, और जो बुनियादी ढांचा वे अभी विकसित कर रहे हैं वह कई दशकों तक चलने वाला है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जीवाश्म-आधारित बुनियादी ढांचे और अक्षय-आधारित बुनियादी ढांचे की बजाय अब ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना सस्ता होने जा रहा है।
इसलिए, एक सुझाव यह है कि, इस इतिहास के निर्भरता के आधार पर, विकासशील देश विकसित देशों के साथ बातचीत शुरू करें। उदाहरण के लिए, इनमें से एक संभावित परिवर्तक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और बढ़ावा देना है। जबकि स्वच्छ विकास और जलवायु परिवर्तन पर यूरोपीय संघ-भारत की पहल एक अच्छा प्रारंभिक कदम है, यह भी स्पष्ट है कि अगर दुनिया कार्बन उत्सर्जन को कम करना चाहती है, तो समय सीमित है। आर्थिक वृद्धि के बावजूद कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, विकासशील देशों को विकसित देशों की सस्ती और अत्यधिक विकसित टिकाऊ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों तक पूरी तरह से पहुंच की जरुरत है; और उन्हें बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाने के लिए पैसों की जरुरत है।
एक और मुद्दा यह है कि विकासशील देशों के पास जलवायु परिवर्तन के प्रति पूर्ण रूप से अनुकूल होने के लिए उपयुक्त साधनों की कमी है, और यह भी की उनका उत्सर्जन उन स्तरों को पार कर जाएगा जो असह्य वार्मिंग की ओर ले जाएंगे। इसलिए, यह भारत जैसे विकासशील देशों के हित में है कि वे शमन पर पूर्ण सहयोग करे, चाहे वह कार्बन मूल्य निर्धारण या वैश्विक कैप-एंड-ट्रेड प्रोग्राम (संभावित इक्विटी समायोजन के साथ) के माध्यम से हो। यह जलवायु उत्सर्जन की समस्या से निपटने के लिए छोटे उत्सर्जन में कमी के साथ एकतरफा अनुकूलन की तुलना में काफी सस्ता तरीका होगा।
नोट्स:
- कैप-एंड-ट्रेड एक नियामक प्रणाली को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है। कैप-एंड-ट्रेड प्रोग्राम के तहत, कुछ प्रकार के उत्सर्जन या प्रदूषकों पर एक सीमा (या 'कैप') तय की जाती है, और कंपनियों को उनकी सीमा के अप्रयुक्त हिस्से को अनुपालन करने के लिए संघर्ष कर रहे अन्य कंपनियों को बेचने (या 'ट्रेड' करने) की अनुमति होती है।
लेखक परिचय: इंगमार शूमाकर फ्रांस स्थित आईपीएजी बिजनेस स्कूल में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उनका शोध पर्यावरण अर्थशास्त्र पर केंद्रित होता है।
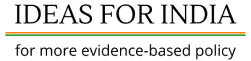

.svg)
.svg)
.svg)

.svg)





























































.svg)

.svg)
%201.svg)
.svg)
.svg)